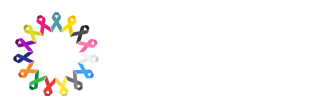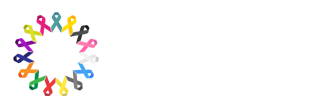बच्चों में ब्रेन ट्यूमर
मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। मस्तिष्क खोपड़ी गुहा के अंदर एक नरम बनावट है और इसमें तंत्रिका कोशिकाएं और दूसरे तरह की कोशिकाएं होती हैं। रीढ़ की हड्डी में रीढ़ के साथ मौजूद एक ट्यूब जैसी बनावट होती है, जो ऊपर मस्तिष्क तक जाती है। वे एक साथ मिलकर सी.एन.एस. या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं।
मस्तिष्क के अंदर बढ़ने वाले ट्यूमर को दिमाग (ब्रेन) का ट्यूमर कहा जाता है और जो रीढ़ की हड्डी के अंदर बढ़ते हैं उन्हें रीढ़ की हड्डी का ट्यूमर कहा जाता है।
ट्यूमर हल्के या घातक हो सकते हैं और इनमें से कुछ आम ट्यूमर नीचे दिए गए हैं।
रक्त संबंधी ट्यूमर के बाद बच्चों में होने वाला दूसरा सबसे सामान्य ट्यूमर ‘प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर’ है। बच्चों में होने वाले ब्रेन ट्यूमर में निम्न और उच्च श्रेणी के ग्लियोमा, मेडुलोब्लास्टोमा, एपेंडिमोमा, क्रैनियोफैरिंजियोमा, जर्म सेल ट्यूमर और नर्व शीथ ट्यूमर शामिल हैं। इनमें सबसे सामान्य नीचे दिए गए हैं।
ब्रेन ट्यूमर की पहचान और लक्षण
इन ट्यूमरों से जुड़े लक्षणों में सिरदर्द, आंखों की रोशनी में बदलाव, दौरा, सुस्ती, भ्रम, चलने फिरने में कमी और कमजोरी जैसे लक्षण शामिल हो सकते हैं। इसकी पहचान एम.आर.आई. स्कैन या मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी के सीटी स्कैन से की जा सकती है। बायोप्सी या ऑपरेशन करके रोग की पहचान पक्की की जाती है।
ग्लियोमा, ग्लियाल कोशिकाओं से विकसित होने वाले मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के ट्यूमर हैं। ये बचपन के कुल ब्रेन ट्यूमर का 30%-40% होते हैं। ये मस्तिष्क में एस्ट्रोसाइट्स बनाते हैं, जिन्हें एस्ट्रोसाइटोमस कहा जाता है, और जो ऑलिगोडेंड्रोग्लिअल कोशिकाओं से बढ़ सकते हैं, उन्हें ऑलिगोडेंड्रोग्लिओमस कहा जाता है। कम स्तर के ग्लियोमा धीमी गति से बढ़ने वाले ट्यूमर हैं।
इन ट्यूमरों के इलाज़ के तरीकों में ऑपरेशन, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी शामिल हैं। आमतौर पर ऑपरेशन सबसे पहला इलाज़ है, अगर ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बुरे प्रभाव पैदा किए बिना ट्यूमर को निकाला जा सकता है। हो सकता है कि ऑपरेशन से ट्यूमर को पूरी तरह से निकाला जा सके। उन रोगियों में जिनमें ऑपरेशन नहीं हो सकता है या जहां ऑपरेशन अधूरा है या जहां ऑपरेशन के बाद कैंसर वापस हो जाता है, वहां बीमारी को नियंत्रित करने में मदद के लिए रेडियोथेरेपी इलाज़ का एक अच्छा तरीका है। रेडियोथेरेपी 6 सप्ताह तक सप्ताह में 5 दिन और दिन में एक बार दी जाती है। अगर रेडियोथेरेपी के बाद बीमारी बढ़ती है, तो कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें इस्तेमाल की जाने वाली आम दवाओं में कार्बोप्लाटिन और विन्क्रिस्टिन शामिल हैं।
ग्लियोमा को कई स्तरों में बांटा गया है। स्तर 1 और 2 को कम स्तर का और स्तर 3 और 4 को बड़े स्तर का कहा जाता है। बड़े स्तर के ट्यूमर ज्यादा गंभीर होते हैं, और वे तेजी से बढ़ते हैं। बड़े स्तर के ग्लियोमा के लक्षण कम स्तर वाले के समान ही होते हैं, सिवाय इसके कि वे कम समय तक के हो सकते हैं। रोग की पहचान को साबित करने के लिए बायोप्सी की जाती है। यदि ट्यूमर उस जगह पर है, जहां ऑपरेशन से ट्यूमर को निकाल सकते हैं, तो ऑपरेशन के बारे में सोचा जाता है। नहीं तो 6 सप्ताह तक दिन में एक बार या सप्ताह में 5 दिन रेडियोथेरेपी का भी एक विकल्प होता है। यहां कार्बोप्लाटिन और टेम्पोज़ोलोमाइड जैसे कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है।
बचपन की एपेन्डीमोमा ज़्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होती है और ये बचपन के कुल ब्रेन ट्यूमर का लगभग 10% होते हैं। ये दिमाग में मौजूद एपेंडिमल कोशिकाओं से पैदा होते हैं।
एपेन्डीमोमास का सबसे बेहतर इलाज़ रेडियोथेरेपी के बाद ऑपरेशन से ही मिलता है। यदि हो सके तो ऑपरेशन से ही इसे ठीक किया जा सकता है। रेडियोथेरेपी मस्तिष्क के उस हिस्से को दी जाती है, जहां ट्यूमर 6 सप्ताह तक मौजूद था। आमतौर पर रेडियोथेरेपी 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जाती है, क्योंकि इससे इन बच्चों के दिमागी विकास पर काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल तब किया जाता है, जब रेडियोथेरेपी नहीं दी जा सकती है या तब, जब ऑपरेशन और रेडियोथेरेपी के बाद भी कैंसर वापस आ जाता है। इस विधि में सिस्प्लैटिन आधारित कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है।
मेडुलोब्लास्टोमा एक कैंसर है, जो दिमाग के सेरिबैलम नाम के भाग में शुरू होता है। यह बच्चों में होने वाला सबसे आम ब्रेन ट्यूमर है। आमतौर पर यह लगभग 5-6 साल की उम्र में होता है।
लक्षण
मेडुलोब्लास्टोमा वाले बच्चों में निम्न लक्षण होते हैं। मेडुलोब्लास्टोमा के रोगियों में सिरदर्द सबसे आम है। ये रात को या एकदम सुबह के समय हो सकते हैं। वे उल्टी, मतली और बदले हुए बर्ताव से जुड़े हो सकते हैं। ये ट्यूमर रोगियों के चलने-फिरने में बदलाव का कारण बन सकते हैं। वे अपने पैरों पर ठीक से खड़े नहीं हो पाते हैं। यह अचानक शुरू हो सकता है या धीरे-धीरे बढ़ सकता है। मेडुलोब्लास्टोमा के रोगियों की नज़र धुंधली हो सकती है या उन्हें चक्कर आ सकता है या नज़र दोहरी हो सकती है। दिमाग में बढ़ते दबाव के कारण रोगी धीरे-धीरे सुस्त हो सकते हैं और होश में रहने में कमी आ सकती हैं।
मेडुलोब्लास्टोमा में जांच
मेडुलोब्लास्टोमा का शक होने पर निम्न टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहले मस्तिष्क का एम.आर.आई. स्कैन किया जाता है। मस्तिष्क में ट्यूमर को देखने के लिए एम.आर.आई. सी.टी. स्कैन से बेहतर है। कटि पंचर एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें रीढ़ में तरल पदार्थ (सी.एस.एफ.) का नमूना लेने के लिए एक सुई को रीढ़ की हड्डी की नलिका में डाला जाता है। इस तरल पदार्थ की मेडुलोब्लास्टोमा कोशिकाओं की मौजूदगी के लिए जांच की जाती है, क्योंकि यह ट्यूमर तरल द्वारा दिमाग से रीढ़ के अन्य भागों में फैल सकता है। ऑपरेशन से ट्यूमर को निकाल दिए जाने के बाद इसकी जांच माइक्रोस्कोप से की जाती है और मेडुलोब्लास्टोमा की पक्की पहचान की जाती है। इसमें अलग से बायोप्सी नहीं की जाती है क्योंकि आमतौर पर ऑपरेशन फिर भी जरूरी होता है और रोग की पहचान करने के लिए एम.आर.आई. अच्छा होता है।
मेडुलोब्लास्टोमा के स्टेज
मेडुलोब्लास्टोमा के स्टेज़ नीचे दिए गए बेहतर चांग माप के अनुसार किए जाते है।
ट्यूमर का फैलाव
| टी1 | 3 सेमी से कम का ट्यूमर |
| टी2 | 3 सेमी से अधिक का ट्यूमर |
| टी3 | 3 सेमी से अधिक का ट्यूमर और सिल्वियस की नलिका जैसे बनावटों और/या लुस्चका के फोरामेन या दिमाग के स्टेम में फैला हुआ। |
| टी4 | 3 सेमी से अधिक का ट्यूमर और सिल्वियस या फोरमैन मैग्नम के नलिका के पास से फैला होता है। |
मेटास्टेस की डिग्री
| एम0 | बड़े मेटास्टेस का कोई सबूत नहीं |
| एम1 | रीढ़ के तरल पदार्थ में पाई जाने वाली छोटी कोशिकाएं (सी.एस.एफ़.) |
| एम2 | दिमाग के अवजालतानिका अवकाश या तीसरे या पार्श्व निलय में देखा गया रोग |
| एम3 | रीढ़ की अवजालतानिका अवकाश में देखा जाने वाला रोग |
| एम4 | दिमाग या रीढ़ के बाहर मेटास्टेस का होना। |
मेडुलोब्लास्टोमा का उपचार
ऑपरेशन, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी सभी को मेडुलोब्लास्टोमा के इलाज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे की उम्र के आधार पर इलाज़ के चुनाव अलग-अलग हैं। 3 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे और जिनकी बीमारी बहुत बड़ी नहीं है, उनके लिए इलाज़ का पहला तरीका ऑपरेशन से दिमाग का कैंसर निकाल देना है। इसके बाद उनके पास कीमोथेरेपी के साथ रेडियोथेरेपी इलाज़ भी है, जिसमें विंसिनस्टाइन, सीसीएनयू और सिस्प्लैटिन जैसी दवाएं शामिल हैं। यह रेडियोथेरेपी पूरे दिमाग और पूरे रीढ़ को दी जाती है। इसे क्रेनियोस्पाइनल विकिरण कहा जाता है। शुरुआती भाग में रेडियोथेरेपी दिमाग और रीढ़ तक दी जाती है और इसके बाद दिमाग को और रेडियोथेरेपी दी जाती है। कीमोरेडियोथेरेपी लगभग 6 सप्ताह तक चलती है। इसके बाद केवल कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है।
3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, रेडियोथेरेपी उस उम्र में बढ़ते दिमाग के नुकसान के खतरे को देखते हुए नहीं किया जाता है। इन बच्चों का इलाज कीमोथेरेपी के बाद किए जाने वाले ऑपरेशन से किया जाता है। यह कीमोथेरेपी दवाओं का एक मेल है। मेटास्टैटिक जैसे बड़े रोग वाले बच्चों में या जिनका इलाज़ नहीं हो सकता, उनमें कीमोथेरेपी के बाद क्रैनियोस्पाइनल रेडियोथेरेपी इलाज़ का एक अच्छा तरीका है।
इलाज़ के दुष्प्रभाव
जैसा कि ऊपर दिए गए इलाज़ के लिए बच्चे छोटे होते हैं, इसलिए इस इलाज़ से बुरे प्रभाव हो सकते हैं। इनमें मस्तिष्क का कम विकास, कम सुनाई देना, रीढ़ पर रेडियोथेरेपी के असर से बच्चे के विकास में कमी, थायरॉयड ग्रंथि के कार्य में कमी और दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियां शामिल हो सकती हैं। बच्चों में इलाज़ के बाद इस तरह के बुरे प्रभावों पर नज़र बनाए रखने के लिए डॉक्टर से नियमित जांच करानी चाहिए।
ये पिट्यूटरी ग्रंथि के पास शुरू होने वाले दिमाग के ट्यूमर हैं। इस ट्यूमर द्वारा उत्पन्न लक्षण मुख्य रूप से आसपास की बनावट पर आम दबाव के असर से होते हैं, जिनमें आंखों की रोशनी में बदलाव जैसे धुंधलापन या दोहरी नज़र, सिरदर्द, सुस्ती आदि शामिल हैं। ऑपरेशन द्वारा इसे ठीक करने का एक बेहतर तरीका है। यदि ऑपरेशन के बाद रोग बच जाता है या फिर से होता है, तो रोग को नियंत्रित करने के लिए रेडियोथेरेपी दी जाती है। यह इलाज़ 6 हफ्ते तक के लिए होता है। दूसरे बचपन के ब्रेन ट्यूमरों की तरह, बहुत छोटे बच्चों में रेडियोथेरेपी नहीं दी जाती है। इलाज़ के बाद, रोगी को पिट्यूटरी ग्रंथि के काम की देख-रेख के लिए खास निगरानी में रखना चाहिए।
ये बच्चों के मस्तिष्क में होने वाले दुर्लभ ट्यूमर हैं। जर्म सेल ट्यूमर वे ट्यूमर हैं जो शरीर के विभिन्न भागों में मौजूद प्रीमिटिव जर्म सेल्स से विकसित होते हैं। कपाल (खोपड़ी) के भीतर के ट्यूमर जीवन के दूसरे दशक में बच्चों में अधिक पाए जाते हैं। उन्हें मोटे तौर पर जर्मिनोमा और नॉन-जर्मिनोमैटस जर्म सेल ट्यूमर में विभाजित किया जा सकता है।
इन ट्यूमर से जुड़े लक्षणों में मस्तिष्क दबाव में वृद्धि होना शामिल है जिससे सिर दर्द, आंखों के लक्षण, उल्टी, नींद न आना जैसी समस्याएँ महसूस की जा सकती हैं। अन्य लक्षणों में पीयूष (पिट्यूटरी) ग्रंथि के क्रियाकलाप में कमी आना शामिल है क्योंकि ये ट्यूमर इस ग्रंथि के करीब होते हैं।
इन ट्यूमर के निदान के लिए सीटी या एमआरआई स्कैन, बीटा-एचसीजी, एएफपी और अन्य के लिए रक्त परीक्षण और ट्यूमर की बायोप्सी की जाती है। आमतौर पर सीएसएफ विश्लेषण भी किया जाता है और यह निदान में सहायता कर सकता है।
इंट्राक्रैनियल जर्म सेल ट्यूमर का उपचार जर्म सेल ट्यूमर के उप-प्रकार पर निर्भर है। एक क्षेत्र तक सीमित जर्मिनोमा वाले मरीजों के मस्तिष्क की रेडियोथेरपी कुल 4-5 सप्ताह तक की जाती है। उन मरीजों में मस्तिष्क और रीढ़ की रेडियोथेरपी की जाती है जिनमें इन क्षेत्रों में ट्यूमर का अधिक फैलाव होता है।
नॉन-जर्मिनोमैटस जर्म सेल ट्यूमर के उपचार में रेडियोथेरपी के बाद कीमोथेरपी शामिल है। कीमोथेरपी में सामान्यतः सिस्प्लैटिन या कार्बोप्लाटिन दवाओं सहित दवाओं के संयोजन का उपयोग होता है। इसे 3-4 महीने के लिए दिया जाता है, और मस्तिष्क और रीढ़ की रेडियोथेरपी के साथ फॉलोअप किया जाता है जो 6 सप्ताह तक रह सकता है।