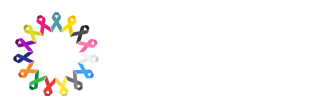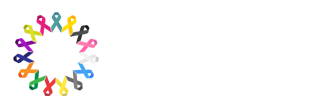मल्टीपल मायलोमा
मल्टीपल मायलोमा क्या होता है ?
मल्टीपल मायलोमा एक प्रकार का कैंसर है जो असामान्य प्लाज्मा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होने के कारण होता है। प्लाज्मा कोशिकाएं एक प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं जो अस्थि-मज्जा में मौजूद होती हैं। अस्थि-मज्जा एक कोमल भाग होता है जो हड्डी के भीतर मौजूद होता है।
जब शरीर पर बैक्टेरिया या वायरस से संक्रमण फैलता है तो प्लाज्मा सेल एंटीबोडी उत्पन्न करते हैं। इन एंटीबोडी को इम्यूनोग्लोबूलिन्स कहते हैं।
इम्यूनोग्लोबूलिन्स पाँच प्रकार के होते हैं जो अपनी विशिष्टताओं के आधार पर विभाजित किए जा सकते हैं। इनके नाम IgA, IgD, IgE, IgM and IgG हैं। ये इम्यूनोग्लोबूलिन्स मुख्य दो भागों के बने होते हैं जो लाइट चेंस और हेवी चेंस कहे जाते हैं। हेवी चेंस ऊपर बताए अनुसार पाँच प्रकार के होते हैं : A, G, D, M, और E और लाइट चेन दो प्रकार होते हैं, कप्पा और लांबड़ा।
जब मायलोमा शरीर में फैलता है तो असामान्य प्लाज्मा सेल्स सामान्यतया कोई एक इम्यूनोग्लोबूलिन को अधिक मात्रा में पैदा करता है। इससे अस्थि-मज्जा में अन्य कोशिकाओं का निर्माण कम हो जाता है जैसे लाल रक्त कोशिकाएं, अन्य सफ़ेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटेलेट्स। अन्य रक्त कोशिकाओं की संख्या में कमी होने और प्लाज्मा कोशिकाओं और असामान्य इम्यूनोग्लोबूलिन्स में वृद्धि से मायलोमा के लक्षण और इसकी वृद्धि हो जाती है। मायलोमा शरीर के विभिन्न हिस्सों में हड्डियों के विनाश का कारण बन सकता है और इससे दर्द होना शुरू होता है तथा फ्रेक्चर भी हो जाते हैं और यह किडनी जैसे शरीर के अंगों को प्रभावित करता है।
आयु
अन्य कई कैंसरों के समान ही मायलोमा में भी बढ़ती हुई आयु एक जोखिम कारक है। 65 की आयु के बाद मायलोमा होना अधिकतर आम बात है।
एमजीयूएस (MGUS)
आकस्मिक एमजीयूएस (MGUS) या मोनोक्लोनल गामोपैथी की स्थिति तब पैदा होती है जब रक्त में पैराप्रोटीन (इम्यूनोग्लोबुलिन) की मात्रा का आधिक्य हो जाता है। कुछ मरीज जिनमें यह स्थिति होती है उनमें एक समयावधि के बाद मायलोमा हो सकता है।
एमजीयूएस (MGUS) के अपने कोई लक्षण नहीं होते और सामान्यतया जब दूसरे कारणों से टेस्ट किए जाते हैं तब संयोग से इनका पता लगता है।
रेडिएशन एक्सपोजर
जहां काम करने जाते हैं या अन्य किन्हीं जगहों पर रेडिएशन के खतरे से मायलोमा विकसित होने का जोखिम बढ़ सकता है।
रोगप्रतिकारक शक्ति का कम होना
कुछ दवाइयां या मेडिकल स्थितियां जैसे एचआईवी/एड्स (HIV/AIDS) के कारण शरीर में रोगप्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है, जो मायलोमा विकसित होने का जोखिम बढ़ा सकती है।
वजन बढ़ना
बढ़े हुए वजन और मोटापे को मायलोमा के विकास के बढ़ते जोखिम से जोड़ा गया है।
ऑटो इम्यून बीमारी
ऑटो इम्यून बीमारी जैसी कुछ स्थितियों में मायलोमा विकसित होने का जोखिम बढ़ जाता है।
मायलोमा शरीर में प्रभावित अंगों के आधार पर कई लक्षण पैदा कर सकता है।
कम ब्लड काउंट होने के लक्षण
जब अस्थि-मज्जा में मायलोमा होता है तो यह सामान्य रक्त कोशिकाएं जैसे लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं और प्लेटेलेट्स घटते जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप यदि लाल रक्त कोशिकाएं कम हों तो मरीज में रक्त की कमी (एनीमिया) और यदि प्लेटेलेट्स कम हों तो खून निकलना और घाव बन जाना और सफेद रक्त कोशिकाएं कम होती हैं तो संक्रमण जैसे लक्षण दिखाई देते हैं।
दर्द होना
मायलोमा शरीर की हड्डियों में फैल जाता है और हड्डियों को कमजोर बना देता है और इन्हें नष्ट भी कर देता है। इससे प्रभावित अंगों में दर्द होता है और हड्डियों का फैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है।
बढ़ा हुआ कैल्शियम
मायलोमा शरीर में खून में कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देता है जिससे थकान, प्यास बढ़ना, पानी की कमी, कब्ज, उल्टियाँ होना और भ्रांति पैदा होने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं।
किडनी को क्षति पहुँचना
मायलोमा प्रोटीन किडनी में जमा होने लगते हैं और इससे गुर्दे का काम करना बंद हो जाता है। इससे पैर में सूझन आना, श्वास लेने में तकलीफ होना, थकान लगना और अन्य लक्षण दिखाई देते हैं।
अन्य लक्षण
मायलोमा के अन्य लक्षणों में अंगों में शिथिलता आना, थकान लगना, भूख कम लगना, वजन कम होते जाना, भ्रांति पैदा होना, चक्कर आना, सिर दर्द होना, मांसपेशियों में कमजोरी, अंगों का सन्न हो जाना और लकवा मार जाना शामिल है।
मरीज में मायलोमा की आशंका होने पर निम्नलिखित टेस्ट किए जाते हैं। इससे निदान करने, मायलोमा के प्रकार का वर्गीकरण और बीमारी फैलने की मात्रा का पता लगाने में मदद मिलती है।
ब्लड टेस्ट
मायलोमा के निदान या उसका पता लगाने के लिए कई प्रकार के ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं। सामान्यतया जो टेस्ट करवाए जाते हैं वे हैं कंप्लीट ब्लड पिक्चर (CBP), किडनी के कार्य का टेस्ट, लिवर के कार्य का टेस्ट (LFT), ईएसआर (ESR), कैल्शियम लेवल और अन्य टेस्ट।
सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस और इम्यूनोफिक्सेशन
यह एक प्रकार का ब्लड टेस्ट है जिसमें बढ़े हुये पैराप्रोटीन अथवा इम्यूनोग्लोबूलिन्स की जांच की जाती है। सीरम इम्यूनोफिक्सेशन से बढ़े हुये पैराप्रोटीन के सही रूप का पता लगाया जाता है।
सीरम फ्री लाइट चेन एस्से
जब लाइट चेन मायलोमा की आशंका होती है तो यह टेस्ट खून में लाइट चेन की मौजूदगी की जांच करने के लिए किया जाता है।
B2 माइक्रोग्लोबुलिन
यह एक मार्कर है जो खून में मौजूद होता है और यह मायलोमा वाले मरीजों में बढ़ जाता है। इस परीक्षण का उपयोग मायलोमा के निदान के साथ-साथ मायलोमा के निदान में उपचार और मदद करने के लिए रोग की प्रतिक्रिया की निगरानी करने के लिए किया जा सकता है।
मूत्र परीक्षण
मायलोमा के निदान में असामान्य प्रोटीन की मौजूदगी के लिए मूत्र के नमूने का परीक्षण किया जाता है।
अस्थि-मज्जा बायोप्सी
मायलोमा के निदान की पुष्टि के लिए अस्थि-मज्जा बायोप्सी की जाती है। प्लाज्मा कोशिकाओं की संख्या की गणना करने के लिए अस्थि मज्जा की जांच की जाती है और आमतौर पर मायलोमा का निदान करने के लिए इसमें 10% या अधिक प्लाज्मा कोशिकाओं की आवश्यकता होती है।
सायटोजेनेटिक्स
अस्थि मज्जा बायोप्सी से नमूने भी कोशिकाओं में आनुवंशिक सामग्री में परिवर्तन के लिए परीक्षण किए जाते हैं जो उपचार के बाद स्थिति के संभावित परिणामों का अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं।
एक्स-रे और स्कैन
हड्डियों में मायलोमा के जमा होने का पता लगाने के लिए हड्डियों का एक्स-रे निकाला जाता है। इस प्रकार के टेस्ट को स्केलेटल सर्वे कहा जाता है। यदि सीटी स्कैन या पीईटी-सीटी स्कैन जैसे स्कैन किए जाते हैं तो स्केलेटन सर्वे की आवश्यकता नहीं होती है। इन परीक्षणों से मायलोमा के निदान और शरीर में बीमारी की मात्रा का पता लगाने में मदद मिलती है।
मायलोमा असामान्य इम्यूनोग्लोबूलिन्स के उत्पन्न होने से होता है। इम्यूनोग्लोबूलिन्स हेवी चेन्स और लाइट चेन्स से बने होते हैं। हेवी चेन्स के विभिन्न प्रकार होते हैं जो G, M, D, A, और E के नाम से जाने जाते हैं।इनमें से सबसे कॉमन है IgG मायलोमा और इसमें उच्च स्तर का इम्यूनोग्लोबूलिन IgG होता है। अन्य प्रकार के हेवी चेन मायलोमा कॉमन नहीं हैं।
एक्टिव मायलोमा
यह मायलोमा सक्रिय होता है और इसके लक्षण भी दिखाई देते हैं। किसी मरीज में मायलोमा है इसका निदान करने के लिए इनमें से कोई लक्षण होना जरूरी है।
अस्थि-मज्जा में 10% से अधिक प्लाज्मा कोशिकाओं का होना
किडनी जैसे अंगों को क्षति पहुँचना और इससे किडनी द्वारा काम करना बंद कर देना
हड्डियों में मायलोमा घाव होना (ओस्टयोलिटिक घाव)
असामान्य रक्त कोशिकाएं जो खून की कमी (अनीमिया), खून बहना अथवा बढ़ा हुआ कैल्शियम स्तर दर्शाते हैं।
लाइट चेन मायलोमा
लाइट चेन में कप्पा और लांबड़ा होते हैं और लाइट चेन मायलोमा या तो कप्पा या लांबड़ा चेन्स निर्मित करते हैं। लाइट चेन मायलोमा सम्पूर्ण इम्यूनोग्लोबूलिन्स निर्मित नहीं करते।
नॉन-सिक्रेटिंग मायलोमा
कुछ मायलोमा बड़ी मात्रा में इम्यूनोग्लोबुलिन्स उत्पन्न नहीं करते हैं जो खून या पेशाब की जांच के दौरान दिखाई नहीं देते हैं, इन्हें नॉन-सिक्रेटिंग मायलोमा कहते हैं।
अज्ञात महत्व के मोनोक्लोनल गामोपैथी (MGUS)
यह वह स्थिति होती है जिसमें प्लाज्मा कोशिकाओं या इम्यूनोग्लुबोलीन (पैराप्रोटीन) की संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन यह वृद्धि इतनी अधिक नहीं होती कि इससे मायलोमा का निदान किया जा सके। ऐसी स्थिति में, मरीज डॉक्टर के गहन निगरानी में रहता है। बहुत कम मरीजों में कुछ वर्षों बाद मायलोमा हो सकता है।
स्मूल्दरिंग मायलोमा
इस स्थिति में मायलोमा का निदान किया जाता है लेकिन मायलोमा से शरीर के अंगों में पहुंची क्षति का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इस स्थिति में, प्रतीक्षा और देखने के दृष्टिकोण को अनुकूलित करना और मायलोमा की वृद्धि होने पर ही इलाज करना संभव है। स्मूल्दरिंग मायलोमा को कम खतरा, मध्यम खतरा और अत्यधिक खतरे में विभाजित किया जा सकता है।
प्लाज्मासाइटोमा
सोलिटरी प्लाज्मासाइटोमा एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर की हड्डी या कोमल ऊतकों में प्लाज्मा कोशिकाओं से निर्मित ट्यूमर होता है। यह उस मायलोमा से भिन्न होता है जो अस्थि-मज्जा और 10% से कम प्लाज्मा कोशिकाओं वाली मज्जा में नहीं होता। कुछ मामलों में कई संख्या में सोलिटरी प्लाज्मासाइटोमास भी दिखाई देते हैं। प्लाज्मासाइटोमा का इलाज मायलोमा से अलग तरीके से किया जाता है। प्लाज्मासाइटोमा वाले कुछ मरीजों में कुछ समय के बाद मायलोमा हो सकता है।
यह बीमारी कितनी अधिक फैल चुकी है और यह किन अंगों में हुई है तथा मरीज की आयु और फ़िटनेस क्या है, इन सब पर निर्भर होता है कि मायलोमा का कौनसा उपचार किया जाए।
प्रतीक्षा करें और देखें अभिगम को अपनाना
कम जोखिम वाले स्मूल्दरिंग या एसिम्पटोमैटिक मायलोमा वाले मरीजों में प्रतीक्षा करें और देखें अभिगम को अपनाया जा सकता है जहां उपचार नहीं दिया जा रहा हो और उनकी 3-6 महीनों में जांच की जानी चाहिए। जब मरीज में मायलोमा के लक्षण दिखाई देने लगें या बीमारी के बढ़ने के साथ साथ लक्षण भी प्रारम्भ हो गए हों तब उपचार प्रारम्भ किया जाता है।
इंडक्शन थेरेपी
एक बार मायलोमा का निदान हो जाने पर डॉक्टर इंडक्शन थेरेपी पर विचार कर सकते हैं। यह उपचार मौजूदा बीमारी को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इंडक्शन थेरेपी औषधियों के विभिन्न प्रकारों के मिश्रण से दी जाती है जिसमें कीमोथेरेपी, बायोलोजिकल एजेंट, स्टीरोइड और अन्य औषधियाँ शामिल हैं। इनका चयन मरीज की हालत और औषधियों की उपलब्धता पर आधारित होता है। इंडक्शन थेरेपी की अवधि 3-6 महीने तक हो सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उच्च खुराक चिकित्सा और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट पर बाद में विचार किया जा रहा है और कैंसर उपचार के लिए कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है।
इंडक्शन थेरेपी देते समय मरीजों को ट्रांसप्लांट के लिए योग्य या अयोग्य के रूप में विभाजित किया जाता है। उन मरीजों को जिन्हें योग्य माना जा रहा है उन्हें बड़ी डोज़ की कीमोथेरपी देने का विकल्प दिया जाता है और उसके बाद स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। इसका विस्तृत ब्योरा नीचे दिया जा रहा है। सामान्यरूप से इंडक्शन उपचार का बेहतरीन प्रभाव डालने के लिए दो या तीन औषधियों का मिश्रण किया जाता है। इन औषधियों के मिश्रण में स्टेरोइड, कीमोथेरपी और बायोलोजिकल थेरेपी शामिल है।
प्रत्यारोपण योग्य मरीजों में इंडक्शन थेरेपी के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य उपचारों में शामिल हैं-
- थैलिडोमाइड अथवा लेनालिडोमाइड और डेक्सामेथासोन
- साइक्लोफोस्फेमाइड, बोर्टेज़ोमीब और डेक्सामेथासोन
- बोर्टेज़ोमीब और डेक्समिथेसोन
- थैलिडोमाइड बोर्टेज़ोमीब और डेक्सामेथासोन
ट्रांसप्लांट के लिए अयोग्य मरीजों में इंडक्शन उपचार में शामिल होता है-
- उपर्युक्त औषधियाँ और उनके साथ साथ जिनमें मेलफालन होता हो जैसे
- बोर्टेज़ोमीब, लेनालिडोमाइड और प्रेड्निसोलोन
- मेलफालन और प्रेड्निसोलोन
अनुरक्षण थेरेपी
इंडक्शन थेरेपी के पूरा होने के बाद जिन मरीजों में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट नहीं किया गया है उनमें अनुरक्षण उपचार पर विचार किया जा सकता है। इसमें इंडक्शन थेरेपी के बाद उपचार जारी रखना शामिल है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के पूरा होने के बाद अनुरक्षण उपचार भी दिया जा सकता है। अनुरक्षण थेरेपी में सामान्यतया प्रयुक्त औषधियाँ बोर्टेज़ोमीब, लेनालीडोमाइड, थैलिडोमाइड या स्टीरोइड होती हैं। यह उपचार सामान्यतया नियमित अंतरालों में दी जानेवाली सिंगल औषधि के रूप में होता है।
कीमोथेरपी
मायोलोमा के उपचार में कीमोथेरपी अकेले या स्टेरोइड और बायोलोजिकल एजेन्टों के मिश्रण में दी जाती है। इस स्थिति में प्रयुक्त कॉमन कीमोथेरपी एजेंट होते हैं साइक्लोफोस्फेमाइड, मेलफालन, डोक्सोरुबीसिन और इदारुबीसिन। कुछ मिश्रणों की सूची नीचे दी गई है।
- साइक्लोफोस्फेमाइड, थैलिडोमाइड और डेक्सामेथासोन (CTD)
- डोक्सोरुबीसिन, बोर्टेज़ोमीब, डेक्सामेथासोन (PAD)
स्टेरोइड
सामान्यतया स्टेरोइड शरीर में उत्पन्न होते हैं और वे शरीर में विभिन्न कार्य करते हैं। कैंसर में उनका प्रयोग सूजन को कम करने के लिए किया जाता है और वे आम तौर पर मायलोमा के उपचार में प्रयोग में लाये जाते हैं। मायलोमा में कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए सीधा प्रभाव डालते हैं। वे अकेले या सामान्यरूप से कीमोथेरपी या बायोलोजिकल थेरेपी के साथ साथ प्रयुक्त होते हैं। इस सेटिंग में प्रयुक्त स्टेरोइड हैं डेक्सामेथासोन, प्रेड्निसोलोन या मिथाइल प्रेड्निसोलोन। स्टेरोइड गोलियों के रूप में या नस में इंजेक्शन के रूप में रोजाना या उपचार चक्र के दौरान कुछ दिनों में दिया जाता है।
बायोलोजिकल एजेंट
बायोलोजिकल एजेंट या निर्धारित थेरेपी वे औषधियाँ हैं जो शरीर के निर्धारित विशिष्ट भाग पर या कैंसर कोशिकाओं पर कैंसर की वृद्धि को रोकने या उसे मारने के लिए प्रयोग में लायी जाती हैं। ये एजेंट सामान्यतया मायलोमा के उपचार में प्रयुक्त होते हैं। वे अकेले प्रयोग में लाये जाते हैं या स्टेरोइड और कीमोथेरपी के मिश्रण में दिए जाते हैं। सामान्यरूप से प्रयुक्त एजेन्टों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- थैलिडोमाइड
- लेनालिडोमाइड
- बोर्टेज़ोमीब
बोर्टेज़ोमीब यह प्रोटीसोम इनहिबिटर्स नामक दवा की ग्रुप से संबंधित दवा होती है। प्रोटीसोम कैंसर कोशिका के वृद्धि में सहायक होती हैं और ये औषधियाँ इस मिकेनिजम को रोकती हैं। बोर्टेज़ोमीब नस में या त्वचा के भीतर इंजेक्शन के रूप में दी जाती हैं।
करफिलजोमीब और इक्साज़ोमीब नयी प्रोटीसोम इनहिबिटर्स हैं, यह उस मायलोमा के इलाज में प्रयुक्त होती हैं जो दूसरे उपचार से ठीक नहीं होता है।
थैलिडोमाइड और लेनालिडोमाइड इम्यूनोमोड्यूलेटिंग एजेंट हैं जिनका प्रयोग मायलोमा के उपचार के लिए होता है। उनमें एंटीएंजियोजेनिक गुण होते हैं जो नयी रक्त-वाहिकाओं के निर्माण को रोकती हैं जो कैंसर की वृद्धि के लिए जरूरी होती हैं। ये औषधियाँ गोलियों के रूप में दी जाती हैं।
उच्च खुराक थेरेपी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट
यह उपचार का एक तरीका है जो उन मरीजों में दिया जाता है जिनमें इंडक्शन थेरेपी का पूरा होने का स्टेज चल रहा हो या उस समय जब प्रारम्भिक उपचार के बाद मायलोमा वापस हो गया हो। इस उपचार में खून और अस्थि-मज्जा में सभी रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए कीमोथेरपी का बड़ा डोज़ दिया जाता है। इसका उद्देश्य शरीर में मौजूद किसी और मायलोमा कोशिका को मारना होता है। उसके बाद जो स्टेम सेल्स बड़े डोज़ की कीमोथेरपी के पहले एकत्रित किए जाते हैं उन्हें वापस मरीज में डाला जाता है और ये कोशिकाएं मरीज में नयी रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये उपचार सभी मरीजों के लिए उपयुक्त नहीं होता और यह मरीज की आयु, फ़िटनेस और मायलोमा के स्टेटस जैसे कारकों पर निर्भर करता है।
अस्थि-मज्जा का सामान्य कार्य लाल रक्त कोशिकाओं जैसी रक्त कोशिकाओं को उत्पन्न करती हैं, जो ऑक्सिजन ले जाने के लिए खून की मदद करती है, सफेद रक्त कोशिकाएं जो संक्रमण से रक्षा करती है और प्लेटेलेट्स जो खून के बहाव को रोकते हैं। खून में इन कोशिकाओं की भारी कमी मरीज के लिए खतरनाक होती है अतः कीमोथेरपी के बड़े डोज़ के बाद इन कोशिकाओं के ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है।
स्टेम कोशिकाओं को एकत्रित करना
स्टेम सेल एक प्रकार की रक्त कोशिकाएं हैं जिनमें लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं अथवा प्लेटेलेट्स जैसी किसी भी प्रकार की रक्त कोशिकाओं को विकसित करने की क्षमता होती है। ये स्टेम सेल्स रक्त प्रवाह और अस्थि-मज्जा में मौजूद होते हैं और मरीज को कीमोथेरेपी का बड़ा डोज़ देने के पहले प्रारम्भ में मरीज से एकत्रित किए जाते हैं। मरीज से स्टेम सेल्स को एकत्रित करने और उसके बाद कीमोथेरपी के बड़े डोज़ के बाद उसे वापस मरीज में डालने की प्रक्रिया को ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कहते हैं।
यदि स्टेम सेल्स दूसरे व्यक्ति (दाता) से लिए जाते हैं तो इन्हें एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कहते हैं। स्टेम सेल दाता कोई रिश्तेदार हो सकता है सामान्यतया भाई या बहन, या रिश्तेदार नहीं हो बल्कि उसका मैच होता हो। दाता की आवश्यकता उन स्थितियों में पड़ती है जब मज्जा में कैंसर हो या पहले ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट किया गया हो लेकिन बीमारी पुनः कष्टदाई बन गई हो।
स्टेम सेल को एकत्रित करने के पहले मरीज द्वारा कीमोथेरपी और G-CSF वाले इंजेक्शन दिये गए हों जो सफल कलेक्शन पाने के लिए खून में पर्याप्त मात्रा में स्टेम सेल की संख्या बढ़ाएगा।
स्टेम सेल को एकत्रित करने के दिन मरीज को एक मशीन से जोड़ दिया जाता है और एक नस से मरीज का खून निकाला जाता है और खून में मौजूद स्टेम सेल को एकत्रित करने के लिए इसे मशीन में से निकाला जाता है। यह खून दूसरी नस के माध्यम से मरीज में वापस डाला जाता है। यह प्रक्रिया कुछ घंटों के लिए चलती है।
एक बार स्टेम सेल एकत्रित कर लेने के बाद मरीज को कीमोथेरपी का एक बड़ा डोज़ दिया जाता है। कीमोथेरपी के बाद स्टेम सेल पुनः मरीज में डाले जाते हैं। ये सेल अस्थि-मज्जा में चले जाते हैं और पुनः ये रक्त कोशिकाएं बनाना शुरू कर देते हैं।
इन दिनों अस्थि-मज्जा ट्रांसप्लांट की तुलना में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट बहुत अधिक प्रयोग में लाया जाता है।
अस्थि-मज्जा को एकत्रित करना
अस्थि-मज्जा एक मुलायम पदार्थ होता है जो हड्डियों के भीतर मौजूद होता है। अस्थि-मज्जा ट्रांसप्लांट के लिए कीमोथेरपी का बड़ा डोज़ देने के पहले मज्जा को एकत्रित करना जरूरी होता है। मज्जा एकत्रित करने की प्रक्रिया सामान्यतया किसी ऑपरेशन थियेटर में जनरल एनेस्थीसिया के तहत की जाती है। हड्डियों के भिन्न भिन्न स्थानों से मज्जा को निकाला जाता है और लगभग एक लीटर जितना इस प्रक्रिया के माध्यम से निकाला जाता है। एक बार निकाल कर इसे संग्रहीत किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर मरीज में डाला जाता है।
स्टेम सेल और अस्थि-मज्जा ट्रांसप्लांट के साइड इफ़ेक्ट्स और जोखिम
स्टेम सेल अथवा अस्थि-मज्जा ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया जटिल होती है इसलिए इसमें साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान सामान्यतया कुछ सप्ताहों के लिए अस्पताल में रहना पड़ता है क्योंकि ट्रांसप्लांट करने के बाद मज्जा में रक्त कोशिकाओं और रक्त को स्वस्थ होने में समय लगता है। इस प्रक्रिया में निम्नानुसार कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं:
मतली आना, उल्टी आना, बालों का झड़ना, लिवर के कार्य में बदलाव ये इस उपचार के संभावित दुष्प्रभाव हैं।
चूंकि सफ़ेद रक्त कोशिकाएं कम हो जाती हैं इसलिए संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और मरीज में जल्दी संक्रमण हो जाता है। यह संक्रमण बेक्टेरिया, वाइरल या फंगल हो सकता है और इसे नियंत्रित करने के लिए सामान्यतया एण्टीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है।
मुंह की भीतरी लाइनिंग और पाचन नली पर कीमोथेरपी के प्रभाव के फलस्वरूप म्यूकोसिटिस हो जाती है। इससे मरीज का भोजन सीमित हो जाता है इसलिए ऐसी स्थिति में भोजन की अन्य पद्धतियों को अपनाया जाता है।
प्लेटेलेट काउंट कम हो जाने से रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है लेकिन प्लेटेलेट काउंट की अधिकता बनाए रखने के लिए प्लेटेलेट ट्रान्स्फ्यूजन दिया जा सकता है।
ग्राफ्ट बनाम होस्ट डिसीज यह ट्रान्स्फ़्युज्ड कोशिकाओं के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया होती है विशेषकर के यदि स्टेम सेल या मज्जा किसी दाता से लिए गए हों।
रेडिओथेरपी
कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए रेडिओथेरपी में अत्यधिक एनर्जी एक्स-रे का प्रयोग किया जाता है। मायलोमा में हड्डियों अथवा शरीर के अन्य भागों में बीमारी के होने से दर्द जैसे लक्षणों के उपचार के लिए रेडिओथेरपी का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतया 1-5 उपचार दिये जाते हैं और वे दर्द को नियंत्रित करने में कारगर होते हैं।
मायलोमा बार बार होने या पुनः होने का उपचार
प्रारम्भिक उपचार के बाद मायलोमा के पुनः होने का उपचार उस पर निर्भर करता है कि यह किस स्थान पर हुआ है, मरीज में कौनसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, मरीज द्वारा पहले क्या उपचार किया गया है और हाल में मरीज के स्वास्थ की फ़िटनेस क्या है। उपचार के विकल्पों में कीमोथेरपी, बायोलोजिकल थेरेपी और सपोर्टिव देखभाल शामिल है।
अन्य उपचार
इस बीमारी या उपचार के कारण जब खून की कमी(एनीमिया) या कम संख्या में प्लेटेलेट होने की स्थितियों में खून ट्रान्स्फ्यूजन, प्लेटेलेट ट्रान्स्फ्यूजन आदि की आवश्यकता हो सकती है।
सोलिटरी प्लाज्मासीटोमा प्लाज्मा सेल के एकत्रित होने का भाग होता है जो कुछ समय के बाद मायलोमा बन जाता है। सोलिटरी प्लाज्मासीटोमा हड्डियों में हो सकता है अथवा शरीर के मुलायम ऊतकों में हो सकता है। मायलोमा के सभी टेस्ट सोलिटरी प्लाज्मासीटोमा किए जाने के पहले किए जाने आवश्यक हैं ताकि मायलोमा की मौजूदगी को दूर किया जा सके।
क्योंकि यह दशा सामान्यतया शरीर के किसी एक भाग में स्थित होती है इसलिए लोकल उपचार जैसे कीमोथेरपी को पसंद किया जाता है। कभी कभी नैदानिक प्रक्रिया के रूप में सम्पूर्ण भाग को सर्जिकल तरीके से काट दिया जाता है। सामान्यतया अन्य टेस्टों के साथ साथ केवल बायोप्सी की जाती है।
प्लाज्मासीटोमा के नियंत्रण के लिए सामान्यतया रेडिओथेरपी उपचार के लिए प्रयोग में लायी जाती है। इस बीमारी को जड़-मूल से निकालने के लिए रेडिओथेरपी 4-5 सप्ताह के लिए दिन में एक बार दी जाती है।
उपचार के पूरा होने के बाद एक समयावधि के बाद मायलोमा फिर से तो नहीं हो रहा इसे जाँचने के लिए क्लीनिक में फॉलो-अप किया जाता है।
मायलोमा का स्टेज निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय स्टेजिंग प्रणाली (ISS), संशोधित आईएसएस (R-ISS) और डुरी-सलमन स्टेजिंग प्रणाली के आधार पर किया जाता है। आईएसएस स्टेजिंग प्रणाली की सूची नीचे दी गई है और यह बीटा 2 माइक्रोग्ल्बुलीन (B2M) और सीरम अल्बूमिन स्तरों पर आधारित होती है और इनका प्रयोग केवल सिम्प्टोमेटिक मायलोमा में ही किया जाता है।
स्टेज 1- B2M स्तर 3.5 mg/l से कम और सीरम अल्बूमिन 3.5 gm/dl के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए।
स्टेज 2- न तो स्टेज 1 न ही स्टेज 3
स्टेज 3- B2M 5.5mg/l के बराबर या उससे अधिक