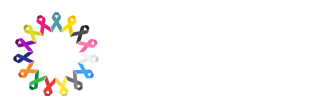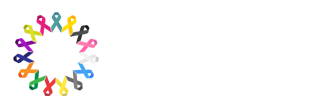न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर
न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम न्यूरोएंडोक्राइन कोशिकाओं से बना होता है। ये कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाओं के समान होती हैं तथा हार्मोन उत्पन्न करती हैं। ये हार्मोन रक्त में घुलकर विभिन्न शारीरिक अंगों पर प्रभाव डालते हैं। न्यूरोएंडोक्राइन कोशिकाएं शरीर के कई अंगों में मौजूद होती हैं। सामान्यतः इन अंगों में आंत, आमाशय, आहारनली, फेफड़े, अग्न्याशय और यकृत शामिल होते हैं।
न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम में विकसित ट्यूमर को न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के सभी ट्यूमरों में लगभग आधे ट्यूमर पाचन तंत्र में होते हैं और उनमें से लगभग एक चौथाई फेफड़े में होते हैं। बाकी शरीर के अन्य अंगों में होते हैं। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर एक असामान्य ट्यूमर हैं, जो औसतन 50-60 साल की उम्र वाले लोगों में होते हैं।
न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर होने का खतरा, उन व्यक्तियों में अधिक होता है, जो अनुवांशिक रोगों, जैसे कि मेन सिंड्रोम, वॉन हिप्पेल-लिंडौ सिंड्रोम, न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस टाइप 1 और टूबेरौस स्क्लेरोसिस से प्रभावित होते हैं। अन्य गंभीर खतरों में धूम्रपान, मधुमेह और क्रोनिक गैस्ट्रिटिस शामिल हैं। क्रोनिक गैस्ट्रिटिस में पेट में सूजन हो जाती है।
क्या न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर ठीक होने वाले (सुसाध्य) ट्यूमर या घातक (कैंसर) होते हैं?
न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर सुसाध्य या घातक ट्यूमर हो सकते हैं। ये किस प्रकार के ट्यूमर हैं, यह उनके प्रकार तथा उनकी वृद्धि की दर पर निर्भर करता हैं, यानी इस बात पर कि, कोशिकाएं कितनी तेजी से विभाजित हो रही हैं। कुछ ट्यूमर बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं और सुसाध्य ट्यूमर की तरह व्यवहार करते हैं जबकि अन्य बड़ी तेजी से बढ़ते हैं एवं घातक ट्यूमर या कैंसर की तरह होते हैं।
न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर की ग्रेडिंग
इन ट्यूमरों को माइक्रोस्कोप से देखे जाने के आधार पर इनमें कोशिकाओं की उपस्थिति के आधार पर 1 से 3 तक का ग्रेड दिया जाता है। Ki-67 इंडेक्स दिया गया है, जो इनका ग्रेड निर्धारित करता है। Ki-67 ट्यूमर में उन कोशिकाओं के अनुपात को देखा जाता है, जो सक्रिय रूप से विभाजित हो रही हैं। कोशिकाएं जितनी अधिक तेजी से विभाजित होती हैं, Ki-67 ग्रेड उतना ही अधिक होता हैं। ग्रेड-1 ट्यूमर की कोशिकाएं, सामान्य कोशिकाओं के समान दिखाई देती हैं एवं धीरे-धीरे बढ़ती हैं जबकि ग्रेड-3 ट्यूमर की कोशिकाएं एक सामान्य कोशिका से बहुत अलग दिखती हैं और बहुत तेजी से बढ़ती हैं।
न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर अगर छोटे हैं, तो उनके लक्षण नहीं दिखते। हाँ ऐसा हो सकता है कि अन्य कारणों से किए गए परीक्षणों में ये संयोग से दिख जाएं। यह लक्षण शरीर में ट्यूमर के स्थान तथा अन्य भागों में विशेष रूप से यकृत में ट्यूमर के प्रसार की दर पर निर्भर करता है। इन ट्यूमरों के लक्षण नीचे संबंधित खंडों में दिए गए हैं।
कार्सिनॉइड सिंड्रोम तब होता है, जब मुख्य रूप से आंत से न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, लीवर में फैल जाता है और इससे ऐसे रसायन (सेरोटोनिन) का स्राव होता है, जो मरीज में विभिन्न प्रकार के लक्षण पैदा करते हैं, जैसे कि दस्त, पेट में दर्द, त्वचा का लाल होना और सूजन, त्वचा का पीलापन और साँस लेने में कठिनाई आदि।
जब न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर होने का संदेह होता है, तो रोग की पुष्टि के लिए कई सारे परीक्षण (जांचें) किए जाते हैं, ताकि ट्यूमर के विशिष्ट प्रकार, यह शरीर के किन-किन भागों में फैला है तथा उपचार के लिए इसकी संभावित प्रतिक्रिया है, आदि बातें जानी जा सकें। इसमें किए जाने वाले आवश्यक परीक्षणों (जांचों) को नीचे दिया गया है।
मूत्र परीक्षण (पेशाब की जांच)
न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर में, सेरोटोनिन जैसे रसायनों का उत्पादन होता है। ये रसायन मूत्र में पाए जा सकते हैं। इनकी जांच से, रोग की पुष्टि के साथ ही उपचार की प्रतिक्रिया का आकलन करने में सहायता मिलती है। मूत्र में परीक्षण किया जाने वाला पदार्थ 5-HIAA या 5 हाईरोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड है। पिछले 24 घंटे में रोगी द्वारा किए गए मूत्र को एक बोतल में एकत्र करके, जांच के लिए लैब (प्रयोगशाला) में भेजा जाता है। इस मूत्र को एकत्र करने से पहले, रोगी को कुछ चीजों से परहेज करने की सलाह दी जाती है, जैसे कि टमाटर, बैंगन, केला, शराब, चाय, कॉफी, अनन्नास, नट के साथ ही ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना है, जिनमें कम मात्रा में सेरोटोनिन पाई जाती हो। मूत्र जिस बोतल में एकत्र की जाती है, वह बोतल लैब द्वारा दी जाती है।
रक्त परीक्षण (खून की जांच)
आमतौर पर, इन ट्यूमरों की पुष्टि में मदद और उपचार की प्रतिक्रिया का आकलन करने के लिए रक्त परीक्षण किए जाते हैं। सीबीपी (CBP), लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन टेस्ट जैसे सामान्य रक्त परीक्षणों के साथ ही क्रोमोग्रेनिन A और B जैसे अन्य परीक्षण किए जाते हैं। यह इन ट्यूमरों द्वारा उत्पादित एक प्रोटीन होता है, और जब इसकी मात्रा खून में बढ़ जाती है, तो यह रोग-निर्णय करने में सहायक होता है। इस परीक्षण का उपयोग, यह देखने के लिए भी किया जाता है कि रोगी पर उपचार का असर हो रहा है या नहीं तथा साथ ही यह भी जानने के लिए कि आरंभिक उपचार के बाद कहीं ट्यूमर फिर से तो नहीं पनप रहा है।
अन्य रक्त परीक्षण, जो किए जा सकते हैं, उनमें इंसुलिन, ग्लूकागन, सेरोटोनिन, गैस्ट्रिन और वीईपी के स्तरों को जानना शामिल है। कुछ विशेष प्रकार के न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमरों में इन रसायनों को उन्नत किया जा सकता है।
अल्ट्रासाउंड स्कैन
छवियों को बनाने के लिए, अल्ट्रासाउंड स्कैन द्वारा ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है तथा इस अल्ट्रासाउंड स्कैनों का उपयोग आम तौर पर, स्तन और अन्य कैंसरों का पता लगाने में किया जाता है। ये स्कैन कम खर्चीले होते हैं तथा इनसे शरीर को कोई हानि नहीं होती, लेकिन कुछ कैंसरों का पता लगाने के लिए, कुछ अन्य स्कैनों जितने, ये कारगर नहीं हो सकते हैं।
सीटी स्कैन
सीटी स्कैन एक प्रकार का स्कैन ही है, जो शरीर के स्कैन किए जाने वाले भाग की त्रि-आयामी छवि बनाने के लिए एक्स-रे का उपयोग करता है। यह कैंसर की पहचान और उसके स्टेज का पता लगाने में, एक एक्स-रे से अधिक उपयुक्त होता है। कंट्रास्ट एन्हांस्ड स्कैन, वह स्कैन है, जिसमें स्कैन करने से पहले, मरीज के नस में एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे बेहतर छवियां मिलती हैं। जब पेट (उदर) का स्कैन किया जा रहा होता है, तो मरीज को ओरल कंट्रास्ट पिलाया जाता है। सीटी स्कैन करने में कुछ ही मिनट लगते हैं। जब कुछ बायोप्सी की जाती है, तो इसमें डॉक्टर के मार्गदर्शन के लिए यानी उसे रोग की स्थिति के बारे में, और अधिक जानने में मदद के लिए सीटी स्कैन का भी उपयोग किया जाता है।
एमआरआई स्कैन
एमआरआई स्कैन में, छवियों को बनाने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है तथा कैंसर की पुष्टि और उसके स्टेज को जानने के लिए, बहुत बार इसका उपयोग किया जाता है। कुछ प्रकार के कैंसरों में यह स्कैन किया जाता है। मस्तिष्क, रीढ़ और श्रोणि (पेट के निचले हिस्से) जैसे शारीरिक भागों में, एमआरआई (MRI), सीटी (CT) स्कैन की तुलना में बेहतर छवियां प्रदान करता है। कुछ मरीजों को एमआरआई स्कैन करवाना मुश्किल होता है, क्योंकि स्कैन करते समय, वे क्लस्ट्रोफोबिक (संवृतिभीत) महसूस करते हैं। एमआरआई स्कैन में 20 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का समय लग सकता है। बेहतर छवियों को पाने के लिए, स्कैन के दौरान, मरीज को कंट्रास्ट एजेंट की सुई लगाई जाती है। कैंसर मरीजों में स्कैन को तारतम्यों (सीक्वेंसों) में किया जाता है तथा एक स्कैन में कई सीक्वेंस किए जाते हैं।
पीईटी-सीटी स्कैन
इस तरह का स्कैन, मानक सीटी स्कैन से अलग होता है, क्योंकि इसमें एक कार्यात्मक तत्व होता है। स्कैन का पीईटी घटक, शरीर के उन भागों का पता लगाने में सक्षम होता है, जहां कैंसर, संक्रमण, सूजन आदि के चलते कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं। कुछ कैंसरों के स्टेज के निर्धारण में सीटी स्कैन से बेहतर, पीईटी-सीटी स्कैन होता है। सबसे पहले, स्कैन के पीईटी भाग को शरीर में रेडिओलेबल्ड पदार्थ को इंजेक्ट करके किया जाता है और फिर स्कैन किया जाता है। इस पदार्थ का उपयोग विभाजित कोशिकाओं द्वारा किया जाता है और इस प्रकार वे स्कैन में दिखती हैं।
पीईटी-सीटी स्कैन की बात करें, तो यह अलग-अलग प्रकार का होता है, तथा किस प्रकार का पीईटी-सीटी स्कैन करना है, यह तेजी से विभाजित हो रही कोशिकाओं को पता करने के लिए प्रयुक्त रेडिओलेबल्ड ट्रेसर के प्रकार पर निर्भर करता है। मानक पीईटी-सीटी स्कैन एक एफडीजी पीईटी (FDG PET) है, जिसमें 18 फ्लोरीन का उपयोग किया जाता है। अन्य उपयोग होने वाले ट्रेसरों में कोलीन सी-11, 11 सी मेथिओनिन, 18एफ लेबल्ड कोलीन, गैलियम 68 लेबल्ड सोमैटोस्टेटिन एनालॉग स्कैन हैं, जिनका उपयोग न्यूरोडोक्राइन ट्यूमर के लिए किया जाता है। आज के समय में, कैंसर तथा इसके सही स्टेज का पता लगाने में सहायता के लिए, आमतौर पर, पीईटी-सीटी स्कैन का उपयोग किया जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि सभी कैंसर पीईटी-सीटी पर दिखाई नहीं देते हैं। अन्य कैंसरों की तुलना में कुछ कैंसर रेडियोएक्टिव ट्रेसर को अपनाते नहीं है और इसलिए, केवल कुछ कैंसरों में ही एक निश्चित जांच के रूप में, पीईटी-सीटी कराने की सलाह दी जाती है।
रेडियोएक्टिव स्कैन
न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमरों की पुष्टि और उपचार में रेडियोएक्टिव ट्रेसरों के उपयोग के साथ युग्मित (जुड़े) स्कैनों का उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ ट्यूमर, इन रेडियोएक्टिव पदार्थों को अवशोषित करते हैं, जिन्हें बाद में स्कैन पर देखा जा सकता है। यह उन छोटे ट्यूमर की पहचान करने में मदद करता है, जिन्हें सामान्य स्कैन के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। उपयोग किए जाने वाले आम रेडियोएक्टिव ट्रेसरों में ऑक्ट्रेओटाइड, mIBG (मेटायोडोबेंज़िलगायनिडाइन), गैलियम डॉटेटेट (पीईटी) शामिल हैं। आमतौर पर, रेडियोएक्टिव पदार्थों को सुई के द्वारा नसों में चढ़ाया जाता है तथा कुछ समय बाद, गामा कैमरा नामक स्कैनिंग मशीन से शरीर के चित्र लिए जाते हैं।
बायोप्सी
न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर की पुष्टि के लिए बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी, एफएनएसी (FNAC) से लेकर कई प्रकार की हो सकती है। एफएनएसी (FNAC) में ट्यूमर में एक छोटी सुई चुभोई जाती है तथा उस ट्यूमर की कुछ कोशिकाओं को कोर बायोप्सी में ले जाया जाता है। फिर यहां, एक बड़ी सुई से ट्यूमर के एक छोटे से भाग का सैंपल लिया जाता है। एक्सिशन बायोप्सी उसे कहते हैं, जिसमें पूरी तरह से हटा दिए गए ट्यूमर का भी उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड स्कैन, सीटी स्कैन की सहायता से बायोप्सी की जाती है, या ट्यूमर की जगह के आधार पर एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी या ब्रोन्कोस्कोपी करके, फिर बायोप्सी की जाती है।
न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर का उपचार शरीर में प्राथमिक ट्यूमर की जगह, उसके प्रकार और शरीर के विभिन्न हिस्सों में उसके हुए प्रसार पर निर्भर करता है। उपचार के मुख्य विकल्पों में निम्न शामिल हैं-
- सर्जरी
- ड्रग थेरेपी
- रेडिएशन थेरेपी
- रेडियोन्यूक्लाइड थेरेपी
- लोकल थेरेपी
सर्जरी
इसका उपयोग विशेषकर उन ट्यूमरों के उपचार के लिए किया जाता है, सर्जरी के लिहाज से छोटे और सामान्य हैं। धीमी गति से बढ़ने वाले तथा एक ही क्षेत्र में सीमित रहने वाले अधिकांश न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमरों में उपचार के लिए विशेष रूप से सर्जरी का उपयोग ही किया जाता है। ट्यूमर और इसके आस-पास के सामान्य ऊतकों को पूरी तरह से निकालना, सर्जरी का मुख्य उद्देश्य होता है। ट्यूमर होने की जगह के आधार पर, सर्जरी विभिन्न प्रकार की हो सकती है।
फेफड़े के ट्यूमर में, सर्जरी करते समय, फेफड़े के एक भाग (एक पालि) या पूरे फेफड़ों को निकाल दिया जाता है। आमाशय के ट्यूमर में, आमाशय का एक भाग या पूरे आमाशय को निकाल दिया जाता है। छोटी या बड़ी आंत के ट्यूमर में, आंत के उस भाग को निकाल दिया जाता है। पित्ताशय और पित्त नली जैसे अग्न्याशय या पित्त पथ के ट्यूमर में, व्हिपल की प्रक्रिया नामक एक ऑपरेशन किया जाता है। ग्रहणी या आमाशय के किसी भाग के ट्यूमर के लिए समान प्रकार की सर्जरी की जाती है। अगर ट्यूमर केवल लीवर में हैं, तो लीवर के उस हिस्से को निकाल दिया जाता है। अगर थायरॉयड ग्रंथि में ट्यूमर है, तो इस ग्रंथि को ही निकाल दिया जाता है।
न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर को हटाने के लिए, की जाने वाली सर्जरी में उसके आस-पास के लिम्फ नोडों को भी निकाल दिया जाता है, ताकि, उनमें ट्यूमर की उपस्थिति का पता चल सके। इससे ट्यूमर के सही स्टेज को अच्छी तरह जानने में तथा उपचार के बाद परिणाम की बेहतरी को बताने में सहायता मिलेगी।
अगर ट्यूमर वाले पूरे भाग को निकाला नहीं जा सकता है, तो इसके कुछ भाग को कम करने के लिए भी सर्जरी की जा सकती है। इससे दवाओं या रेडियोथेरेपी जैसे अन्य उपचारों की प्रभावशीलता को बढ़ाने में मदद मिलती है। कुछ मरीजों में, जिनमें ट्यूमर शरीर के विभिन्न हिस्सों में फैल गया होता है, उनमें कैंसर से संबंधित लक्षणों को सुधारने में मदद के लिए भी सर्जरी की जा सकती है।
दवा उपचार
न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर या कैंसर के इलाज के लिए दवाओं का उपयोग किया जाता है, जिससे ट्यूमर के लक्षणों को सीमित करके इसे नियंत्रण में रखा जाता है।
सोमाटोस्टैटिन एनालॉग्स दवाओं का एक समूह है, जिनका उपयोग आमतौर पर कार्सिनॉइड सिंड्रोम के उपचार में किया जाता है। यह सिंड्रोम तब होता है, जब मुख्य रूप से, आंत से एक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर फैलकर लीवर में पहुंच जाता है और ऐसे रसायन (सेरोटोनिन) पैदा करता है, जो मरीज में विभिन्न लक्षण पैदा करते हैं। इन लक्षणों में दस्त, पेट दर्द, त्वचा का लाल होना और सूजना, सांस फूलना और सांस लेने में कठिनाई आदि शामिल हैं।
आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले सोमाटोस्टेटिन एनालॉग्स ऑक्ट्रोटाइड और लैनरेओटाइड हैं। दोनों दवाओं को इंजेक्शन द्वारा त्वचा में दिया जाता है। ऑक्ट्रोटाइड का एक शार्ट एक्टिंग रूप होता है और इसे रोज देने की जरूरत होती है, जबकि इसके लांग एक्टिंग रूप को हर 4 हप्ते में एक बार देना होता है। लैनरेओटाइड का केवल लांग एक्टिंग रूप ही होता है, और इसे हर 4 हप्ते में एक बार देना होता है।
कीमोथेरेपी का उपयोग, आमतौर पर, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर में कम किया जाता है। यह मुख्य रूप से उन हाई ग्रेड वाले ट्यूमरों में प्रभावी होता है, जो तेजी से बढ़ते हैं और कैंसर का रूप लेने की ओर अग्रसर होते हैं। कीमोथेरेपी का उद्देश्य ट्यूमर को नियंत्रित और लक्षणों में सुधार करते हुए मरीज की जीवनी शक्ति को बढ़ाना होता है।
जैविक दवा या टार्गेटेड थेरेपी में उन दवाओं का उपयोग शामिल है, जो कैंसर कोशिकाओं में विशेष क्षेत्रों को लक्षित करती हैं और जिनका प्रयोग कुछ प्रकार के न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमरों में किया जा सकता है। रोग को नियंत्रित करने के लिए तथा लक्षणों में सुधार के साथ ही, मरीज को जिंदा रखने में सहायता के लिए, इस सेटिंग में एवरोलिमस और सुनिटिनिब जैसी दवाओं का उपयोग किया जाता है।
रेडियोथेरेपी
एक रैखिक त्वरक का उपयोग करके एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी के रूप दी जाने वाली रेडियोथेरेपी का उपयोग कुछ न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमरों, और वह भी, जो विशेष रूप से अस्थियों (हड्डियों) में फैल गए होते हैं, उनमें किया जाता है। उपचार हड्डियों में उत्पन्न होने वाले दर्द को कम करने में मदद करता है।
रेडियोन्यूक्लाइड थेरेपी
यह लक्षित रेडियोथेरेपी है, जिसे उस रेडियोआइसोटोप का उपयोग करके किया जाता है, जिसमें ये अणु ट्यूमर या कैंसर कोशिका से जुड़े होते हैं। जब ऐसी दवाएं दी जाती हैं, तो उन्हें ट्यूमर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और रेडियोन्यूक्लाइड ट्यूमर कोशिका के आसपास के क्षेत्र में विकिरण फैलाकर इन्हें मार देता है या नष्ट करता है। इस तरह के उपचार को पेप्टाइड रिसेप्टर रेडिओलिगैंड थेरेपी (PRRT) भी कहा जाता है।
इससे पहले कि इस तरह के उपचार पर विचार किया जाए, सोमाटोस्टैटिन के साथ रेडियोन्यूक्लाइड स्कैन, यह देखने के लिए किया जाता है कि ट्यूमर सोमाटोस्टेटिन को लेता है या नहीं। यदि यह इसे स्वीकार करता है, तो ये उपचार कारगर हो सकते हैं।
आमतौर पर किए जाने वाले उपचार की बात करें, तो ये लुटेटियम Lu -177 डॉटेटेट और येट्रियम-90 डॉटाटॉक हैं। किस दवा का उपयोग करना है, यह सेंटर में कंपाउंड (यौगिक) की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अगर मरीज को दवा से फायदा होता है, तो इन दवाओं के द्वारा उपचार बार-बार किया सकता है।
लोकल उपचार
न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के उपचार का विकल्प अधिकतम रोग के फैलाव वाले क्षेत्र का उपचार करना होता है। इस विकल्प का उपयोग मुख्य रूप से तब किया जाता है, जब रोग विशेष रूप से लीवर में मौजूद होता है।
हेपेटिक धमनी एम्बोलिज़ेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें दवा को लीवर (यकृत) के उस हिस्से में रक्त की आपूर्ति प्रदान करने वाली धमनी में इंजेक्ट किया जाता है, जिसमें ट्यूमर का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। यह इंजेक्शन धमनी को अवरुद्ध करेगा तथा ट्यूमर को होने वाले रक्त एवं पोषक तत्वों की आपूर्ति को रोककर इसके आकार को कम करेगा। ट्यूमर तक कीमोथेरेपी को पहुंचाने के लिए, कीमोथेरेपी दवाओं को यकृत धमनी में इंजेक्ट किया (सुई के माध्यम से दिया) जा सकता है। इसे कीमोइम्ब्लोइज़ेशन कहा जाता है।
रेडियोइम्ब्लोइजेशन एक वैसी ही प्रक्रिया है, जिसमें ट्यूमर को रेडियोथेरेपी देने के लिए, रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड को सीधे यकृत धमनी में इंजेक्ट किया जाता है।
रेडियोफ्रीक्वेंसी एब्लेशन में लीवर (यकृत) में रोगग्रस्त स्थानों पर रोग को नष्ट करने के लिए रेडियोफ्रीक्वेंसी द्वारा गर्मी (हीट) को ट्यूमर तक पहुंचाया जाता है।
इनमें से किन उपचारों का चयन करना है, यह लोकल विशेषज्ञता और उसकी उपलब्धता पर निर्भर करेगा।